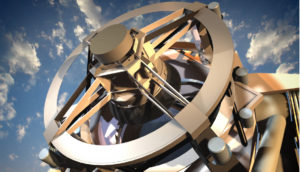इस डरावनी आस्था से सावधान !

विजयदान देथा की एक कहानी है- ‘रिजक की मर्यादा’. जिसमें डरावनी आस्था का ऐसा उदाहरण मिलता है जो आंखें खोलने वाला है. हम सभी को इस कहानी को पढ़ना चाहिए.
कहानी में एक भांड होता है जो तरह-तरह के रूप धर सकता है. वह एक सेठ के यहां साधु बन कर पहुंचता है. सेठ सपरिवार उसका भक्त हो जाता है. अगले कुछ महीनों में यह भक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि सेठ अपनी सारी संपत्ति साधु बने भांड को दान कर देता है!
लेकिन यहां भांड अपने असली रूप में आ जाता है- मैं कोई साधु थोड़े हूं. सेठ सिर पीट लेता है.
फिर पूछता है कि ‘जब तुझे इतनी दौलत मिल गई थी तो तूने फिर साधु वेश छोड़ा क्यों?’
भांड का जवाब है- ‘यह रिजक की मर्यादा है’. रिजक- यानी रिज़्क.
कहानी में आगे यही भांड रानी के कहने पर नया रूप धर कर उसके अत्याचारी भाई को मार डालता है और अंत में ख़ुद मारा जाता है. उसने जान देकर अपने रिज़्क की लाज रख ली.
डरावनी आस्था यह होती है! उसके लिए जान लेने से ज़्यादा ज़रूरी जान देना होता है.
टीएस इलियट के ‘मर्डर इन द कैथेड्रल’ में कैंटरबरी के आर्कबिशप थॉमस बेकेट, इस आस्था के लिए जान दे देते हैं.
यह चीज़ उनके लिए इतनी बड़ी है कि वे हर प्रलोभन ठुकराते हैं- शहीद कहलाए जाने का प्रलोभन भी!
फ़िल्म ‘मुगले आज़म’ की शूटिंग के दौरान अकबर की भूमिका कर रहे पृथ्वीराज कपूर, तपती रेत में चल कर अजमेर में ख़्वाजा चिश्ती की दरगाह तक गए थे. हालांकि फिल्म के निर्देशक के आसिफ़ का कहना था कि वे त्वचा के रंग वाले मोजे पहन सकते हैं.
लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि ‘जब अकबर यहां आया होगा तो क्या वह जूते पहन कर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक गया होगा?’
डरावनी आस्था असल में यह होती है!
उसका वास्ता धार्मिक आडंबरों से या कर्मकांडों से नहीं होता. वह अपने भीतर से पैदा होती है.
वह किसी ईश्वर के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी कर्म के प्रति हो सकती है.
गुरदयाल सिंह का उपन्यास है ‘परसा’.
परसा अपने खेतों में काम करता हुआ सबद और कीर्तन गाता रहता है. वह बहुत आस्थावान सिख है. लेकिन वह कर्मकांडों में नहीं फंसता. हालांकि जब उसके बेटे अपने केश कटवा लेते हैं तो वह दुखी होता है- इस बात से नहीं कि उन्होंने केश कटवाए, बल्कि इस बात से कि यह काम बिना सोचे-विचारे किया.
ग्राहम ग्रीन का एक उपन्यास है- ‘हार्ट ऑफ़ द मैटर’.
उपन्यास का नायक स्कोबी बहुत ईमानदार और सच्चा ईसाई रहता है लेकिन अंत में खुदकुशी कर लेता है, जो ईसाइयत में बहुत बड़ा अपराध है.
उसकी पत्नी चर्च के फादर से कहती है कि चर्च तो स्कोबी को जानता था. फ़ादर रेक्स कहते हैं- ‘हां, चर्च सबकुछ जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि एक अकेले हृदय के भीतर क्या कुछ चल रहा होता है?’
ये सारी कहानियां हैं- आज की नहीं, बीते ज़मानों की.
इंसान के विवेक से निकली हुई, उसकी संवेदना से छन कर आई हुई. ऐसी कहानियां और भी हैं.
ये सारी कहानियां आस्था के सवाल से जूझती हैं. अनास्था का भी सामना करती हैं.
आल्बेयर कामू का उपन्यास ‘आउटसाइडर’ दूसरे विश्वयुद्ध के बाद एक गहरी अनास्था से गुज़र रहे यूरोपीय मानस के बीच से निकला है. उपन्यास के आख़िरी हिस्सों में मृत्यु दंड पाया नायक, अपने पास आए पादरी को जम कर फटकारता है और कहता है कि ‘उसे कोई नकली शांति नहीं चाहिए!’
महाभारत के अठारहवें दिन से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक के काल की कथा कहती काव्य कृति धर्मवीर भारती के ‘अंधा युग’ में कृष्ण को वंचक बताती गांधारी के लिए विदुर कहते हैं-
‘यह कटु निराशा की
उद्धत अनास्था है.
क्षमा करो प्रभु!
यह कटु अनास्था भी अपने
चरणों में स्वीकार करो!
आस्था तुम लेते हो
लेगा अनास्था कौन?’
डरावनी आस्था और अनास्था के सदियों से चले आ रहे द्वंद्व के बीच सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का असली मक़सद इंसान और इंसानियत की तलाश रहा है.
इस तलाश में आस्था की छेनी से ईश्वर बार-बार गढ़े और तोड़े गए हैं, धर्म बार-बार परिभाषित और पुनर्परिभाषित किए गए हैं और बार-बार यह प्रमाणित हुआ है कि अंततः यह संवेदना और विवेक है जिसके साझे से मनुष्यता का रसायन बनता है.
लेकिन आज के हिंदुस्तान में ये सारी कहानियां भुला दी गई हैं.
एक डरावनी आस्था जैसे अट्टहास करती ख़ून बहाती घूम रही है.
कहीं गो-तस्करी के नाम पर, कहीं मोहम्मद साहब के अपमान के प्रतिशोध के लिए, कहीं बस अपनी पहचान न बताने के जुर्म में, और कहीं बस पहचान खुल जाने के अपराध में–कोई भी सिरफिरा किसी का भी गला काट सकता है, पीट-पीट कर उसकी हत्या कर सकता है!
इसके बाद का अनुष्ठान मीडिया और नेताओं के हिस्से आता है.
टीवी चैनलों पर चल रही खोखली और सरोकार विहीन बहसें, बस, देश का तापमान बढ़ाने के काम आती है.
रही-सही कसर वह राजनीति पूरा कर देती है जिसे सांप्रदायिक नफ़रत का यह खेल रास आता है.
इस बर्बर हिंदुस्तान को न मोहम्मद साहब की कथाएं मालूम हैं और न भारत में देवी-देवताओं के वे सैकड़ों रूप, जो बरसों नहीं, सदियों की कल्पना के सांचे में ढले हैं!
मसलन, मोहम्मद साहब की यह कहानी काफ़ी दिलचस्प है:
‘एक रोज उनके तमाम अहम साथियों में से एक साथी मुआज को उन्होंने यमन का सूबेदार बनाकर भेजा. यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी, तो उन्होंने मुआज से जानना चाहा कि जब तुम यमन जाओगे तो तुम्हारा काम करने का तरीका क्या होगा? वह कौन सी बात होगी, जिसकी रोशनी में तुम वहां के लोगों के साथ इंसाफ़ कर सकोगे?
मुआज ने हजरत साहब को बताया कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान कुरआन की शिक्षाओं के आधार पर करेंगे.
हजरत मोहम्मद ने पूछा कि अगर कुरआन की शिक्षाओं के साथ वहां की समस्याओं का तालमेल नहीं बैठा, तब क्या करोगे?
तब मुआज ने कहा कि तब अपने पैगंबर की मिसाल सामने रखकर उन समस्याओं का हल निकाला जाएगा.
हजरत मोहम्मद फिर पूछा कि अगर वह भी उनके साथ ठीक नहीं बैठी, तब क्या करोगे?
मुआज ने जवाब दिया कि तब अपनी अक्ल और इंसाफ को आगे रखकर काम किया जाएगा.
फिर हजरत मोहम्मद मुस्कुराए और बोले कि “यही सबसे अच्छा रास्ता है.”
अपनी अक्ल का इस्तेमाल हर रास्ते से बेहतर है.
हर बात दूसरे के कहने की ही बेहतर नहीं मान लेनी चाहिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बड़े काम अंजाम दिए जा सकते हैं.(सुनन अबी दाऊद 3592)
मुश्किल ये है कि हजरत मोहम्मद के अनुयायी ही यह कहानी भूल गए हैं. उनको लगता है कि मोहम्मद साहब पर की जाने वाली छींटाकशी वाकई उनके गिरेबान तक पहुंच जाएगी. उनको वे कहानियां भी याद नहीं हैं जब कोई चिड़चिड़ी औरत उनके ऊपर सब्ज़ियों के छिलके फेंका करती थी या कोई और किसी अन्य तरह की गुस्ताख़ी करता था जिन्हें वे न सिर्फ़ माफ़ करते थे, बल्कि उनका हालचाल लेने भी पहुंच जाते थे.
मुसलमान अगर मोहम्मद साहब की तालीम भूल गए हैं तो हिंदू तो अपने सारे देवी-देवताओं को बस मूर्तियों तक महदूद मान बैठे हैं.
इस हिंदुस्तान में तो जितने देवी-देवता हैं, उनसे ज़्यादा उनके रूप और नाम हैं.
हर देवी-देवता के साथ तरह-तरह की कहानियां जुड़ी हैं जिनमें कभी उनकी दुर्बलता भी दिखती है और कभी उनकी शक्ति भी. एक पूरी की पूरी दुनिया हमने देवताओं की बसाई हुई है जिसमें किसी की तपस्या से इंद्र का आसन डोलने लगता है और किसी की तपस्या से देवता इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे भस्मासुर बना देते हैं!
शंकर रावण को वरदान देते हैं और संहार मचाती काली को रोकने के लिए शिव उनके सामने लेट जाते हैं!
भारत में देवी-देवताओं की यह विहंगम अनूठी दुनिया शायद सदियों में बनी होगी- तरह-तरह की कहानियों, कविताओं, क़िस्सों, कथाओं, पुराणों-उपनिषदों में लिपटी हुई.
लगभग हर कहानी यही बताती है कि अतिरेक भक्ति का हो, आस्था का हो, वरदान का हो, भगवान का हो, अंततः ख़तरनाक और आत्मघाती होता है!
फिर इस अतिरेक से मुक्ति के लिए देवताओं को धरती पर उतरना पड़ता है.
लेकिन (लगता है) हम जैसे अतिरेकों के आसमान में जी रहे हैं. अपनी धार्मिक पहचान की बहुत सारी परतों को हम खुद नष्ट करने पर तुले हैं.
हमें बस एक राम कथा चाहिए- “एक हज़ार रामायणें” नहीं, जो हमारी दुनिया को अलग सी विविधता और उदारता प्रदान करती हैं.
शिव, विष्णु, काली, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, ब्रह्मा- इन सबकी पूजा हम करते हैं, लेकिन जो इन देवी-देवताओं ने बताया, वह जानने-समझने को तैयार नहीं होते.
हमारे पास होती हैं तो बस विध्वंस की कहानियां होती हैं, निर्माण के नाम पर हम भव्यता की अतिरिक्त भूख के मारे हैं, यह भी नहीं देखते कि जो मूर्तिशिल्प है, जो वास्तुशिल्प है, उसमें कितने धर्मों, कितनी सभ्यताओं का पानी मिला हुआ है.
कृपया यह न समझें कि यह लेख धर्म के पवित्र मूल्यों की याद दिलाने के लिए लिखा जा रहा है या फिर ईश्वर के उस उदार रूप की कल्पना के लिए लिखा जा रहा है जिसे हम खो चुके हैं.
इस टिप्पणी का मक़सद बस यह याद दिलाना है कि सभी धर्म अपने सांगठनिक स्वरूप में राजनीति के अनुगामी हैं और अपने सत्ता विमर्श में इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है.
इन धर्मों का इस्तेमाल एक-दूसरे को लड़ाने, उनको पराया साबित करने के लिए हो रहा है.
देवता बस संहार के रह गए हैं, सृजन के नहीं!
दरअसल जिसे हम धर्म कहते हैं, वह एक अर्थ में साहित्य है!
राम और कृष्ण, शिव और काली के प्रति हमारी जो आस्था है, वह उनकी रचनात्मक स्मृति से है, इस विश्वास से है कि वे हमारी रक्षा करेंगे.
इस विश्वास को ठीक से समझ न पाने का नतीजा है कि धर्म राजनीति से कहीं ज़्यादा निरंकुश हो चुका है और वह देवताओं को पत्थर की मूर्तियों की तरह, अपने अहंकार और अधिकार के प्रतीकों का तरह इस्तेमाल कर रहा है.
अगर हममें धर्म के प्रति सच्ची आस्था होती तो वह आस्था हर क़दम पर ठोकर खाती, हमारी धार्मिक भावना जगह-जगह आहत होती, लेकिन वह धार्मिक भावना नहीं है, आस्था नहीं है, बस “आस्था का दिखावा” है इसलिए वह अवसर देखकर प्रगट होती है.
यह खतरनाक डरावनी आस्था है!
ज़्यादा बुरा यह है कि इस डरावनी आस्था को कई स्तरों पर बढ़ावा मिल रहा है, इसे उकसाया जा रहा है जैसे वही इकलौती आस्था हो और भारत उसके विशेषाधिकार का क्षेत्र हो!
जबकि भारत अपनी सांस्कृतिक बहुलता, भाषिक विविधता, सैकड़ों देवी-देवताओं, हज़ारों आस्थाओं, इससे भी ज़्यादा–पूजा पद्धतियों, तरह-तरह के अजीब रीति-रिवाजों के बीच बसता है.
वह रोज़ एक-दूसरे को देखता और जानता है कि सबको साथ जीना है.
साथ जीने का यह भरोसा अगर कम पड़ा तो हिंदुस्तान कुछ फीका हो जाएगा.
भारत माता के कुछ बेटे पराये माने जाएंगे तो वह कुछ उदास हो जाएगी- दुर्भाग्य से यह समझ उनको नहीं है जो भारत माता का सबसे ज़्यादा नाम लेते हैं!